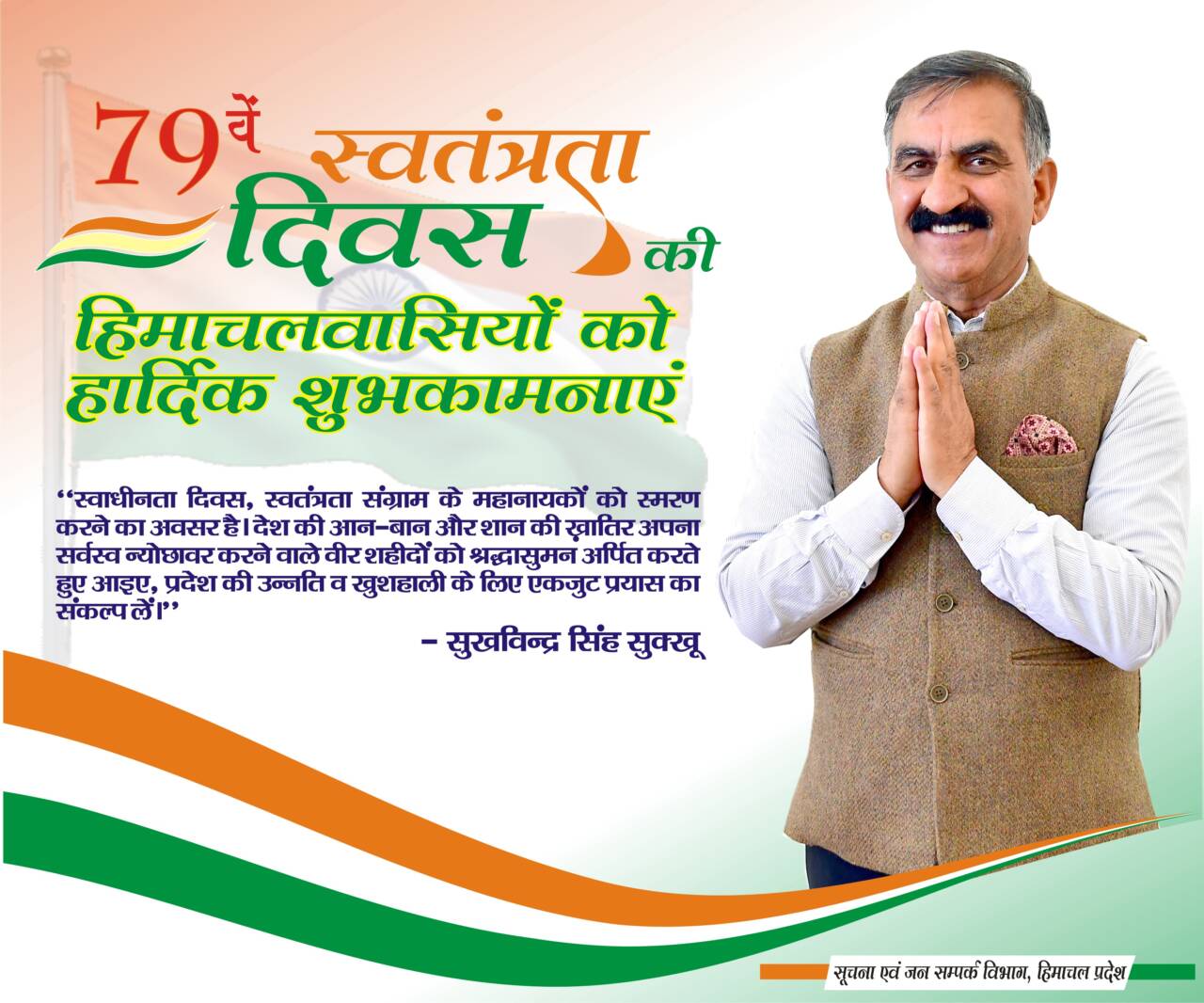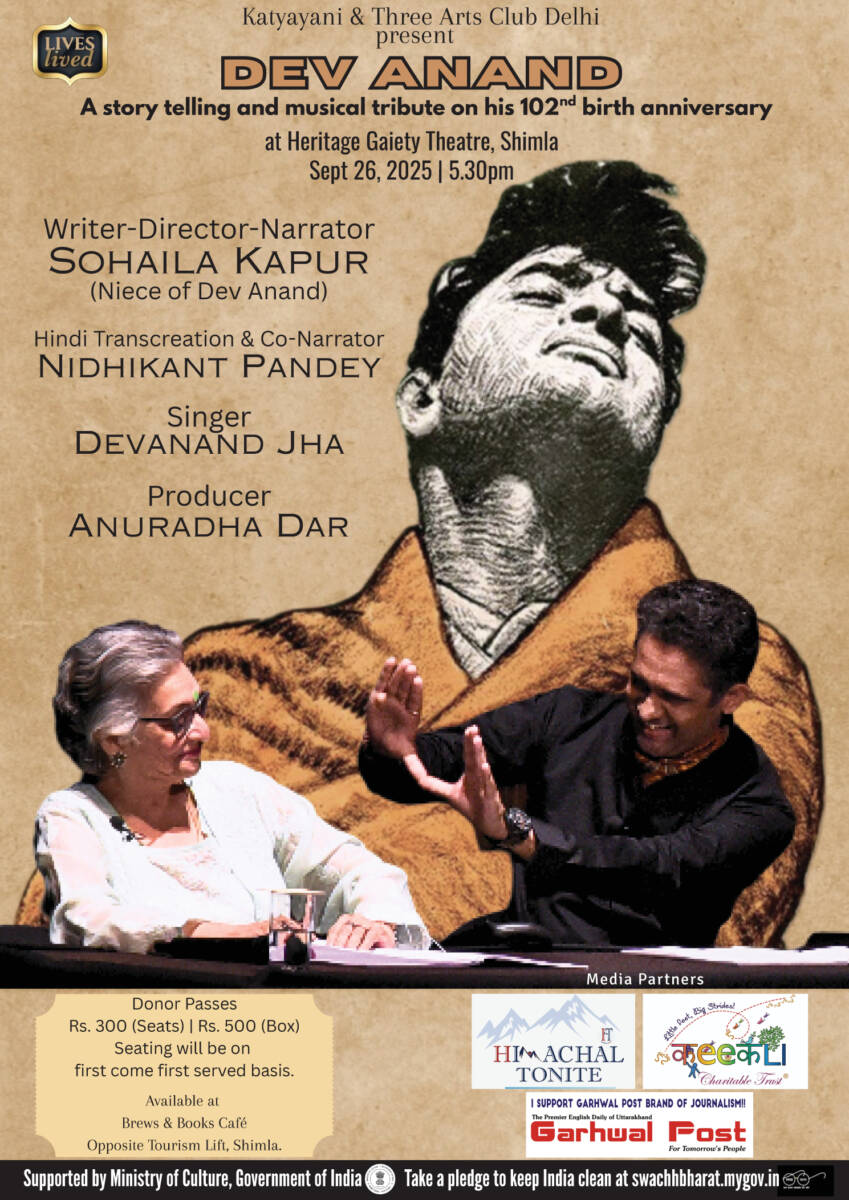सीताराम शर्मा सिद्धार्थ, शिमला
सीताराम शर्मा सिद्धार्थ, शिमला
मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने दोषों को नज़रअंदाज़ करता है और दूसरों की कमियों को बढ़ा-चढ़ाकर देखता है। इसी प्रवृत्ति को छिद्रान्वेषण अथवा परदोषदृष्टि कहा जाता है, जो मानसिक समस्या का रूप ले सकती है। यह प्रवृत्ति समाज में नकारात्मकता और तनाव को जन्म देती है, जिससे न केवल व्यक्तिगत संबंध प्रभावित होते हैं, बल्कि सामाजिक ताना-बाना भी कमजोर होता है।
परदोषदृष्टि का मनोवैज्ञानिक आधार
परदोषदृष्टि मूलतः आत्मरक्षा की एक मानसिक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को स्वीकार नहीं कर पाता, तो वह अपने दोषों का प्रतिबिंब दूसरों में देखने लगता है। यह प्रवृत्ति निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हो सकती है:
हीन भावना: जब व्यक्ति स्वयं को असफल या अयोग्य महसूस करता है, तो वह दूसरों की गलतियों को उजागर कर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने की कोशिश करता है।
अहंकार: कुछ लोग अपने अभिमान के कारण दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उनकी कमियों की ओर इशारा करते हैं।
संस्कार एवं परवरिश: यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक वातावरण में बड़ा हुआ है, जहाँ आलोचना करना आम बात हो, तो वह भी वैसा ही व्यवहार करने लगता है।
समाज का प्रभाव: निंदा और आलोचना की प्रवृत्ति जब समाज में एक प्रचलन बन जाती है, तो व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करता है।
मनोविश्लेषकों के विचार
मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड के अनुसार, परदोषदृष्टि ‘प्रोजेक्शन’ का एक रूप है, जिसमें व्यक्ति अपनी अवचेतन भावनाओं को दूसरों पर थोपता है। कार्ल जुंग के अनुसार, व्यक्ति अपने भीतर के ‘शैडो सेल्फ’ को पहचानने में असमर्थ होता है, इसलिए वह अपनी नकारात्मकताओं को दूसरों में देखने लगता है। आधुनिक मनोविश्लेषक डॉ. जॉर्डन पीटरसन मानते हैं कि आत्मचिंतन और व्यक्तिगत जिम्मेदारी अपनाने से इस प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है।
परदोषदृष्टि के दुष्परिणाम
परदोषदृष्टि की प्रवृत्ति व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न कर सकती है:
व्यक्तिगत संबंधों में खटास: जब व्यक्ति हर समय दूसरों की गलतियों की ओर ध्यान देता है, तो उसके रिश्तों में तनाव बढ़ जाता है।
नकारात्मक मानसिकता: नकारात्मकता से भरी मानसिकता व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से रोक सकती है।
अवसाद एवं चिंता: निरंतर दूसरों की कमियाँ देखने और आलोचना करने से व्यक्ति स्वयं मानसिक तनाव में रहने लगता है।
सामाजिक विभाजन: यह प्रवृत्ति समाज में द्वेष, वैमनस्य और आपसी कलह को बढ़ावा देती है।
धार्मिक एवं आध्यात्मिक गुरुओं के विचार
श्रीकृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, “उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्।” अर्थात, व्यक्ति को स्वयं का उद्धार करना चाहिए और अपनी आत्मा को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। परदोषदृष्टि से बचने के लिए आत्मनिरीक्षण और भक्ति मार्ग का अनुसरण आवश्यक है।
गौतम बुद्ध ने कहा था, “स्वयं का आत्मज्ञान ही व्यक्ति को बाहरी दोष देखने से रोक सकता है।”
स्वामी विवेकानंद के अनुसार, “यदि हम दूसरों में अच्छाई देखने की आदत डालें, तो न केवल हमारी मानसिकता बदलेगी, बल्कि समाज में भी सकारात्मकता फैलेगी।”
संगति का प्रभाव और समाधान
मनुष्य की संगति का प्रभाव उसकी मानसिकता पर गहरा पड़ता है। यदि व्यक्ति नकारात्मक लोगों के बीच रहता है, जहाँ निंदा और आलोचना का माहौल है, तो उसकी सोच भी नकारात्मक हो सकती है। इस से बचने के लिए कुछ निम्लिखित उपाय किए जा सकते हैं:
सकारात्मक संगति बनाएँ
उन लोगों के साथ रहें जो प्रेरणादायक हों और आत्मविकास पर ध्यान देते हों।
निंदा से बचें: यदि किसी समूह में हर समय दूसरों की आलोचना की जाती है, तो ऐसे माहौल से दूरी बनाना उचित रहेगा।
संतुलित दृष्टिकोण अपनाएँ: अपनी संगति में ऐसे लोगों को शामिल करें जो आलोचना के बजाय समाधान केंद्रित दृष्टिकोण रखते हों।
बच्चों को परदोषदृष्टि से बचाने के लिए माता-पिता क्या करें?
उदाहरण बनें: बच्चे अपने माता-पिता से सीखते हैं। यदि माता-पिता दूसरों की गलतियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो बच्चे भी इस प्रवृत्ति से बचेंगे।
सकारात्मक सोच विकसित करें: बच्चों को दूसरों की अच्छाइयों की पहचान करना सिखाएँ और सहानुभूति का भाव विकसित करें।
समस्या समाधान की मानसिकता विकसित करें: केवल दोष देखने के बजाय समस्याओं के हल ढूँढने की आदत डालें।
कहानियों और शिक्षाओं से मार्गदर्शन दें: धार्मिक और नैतिक कथाएँ सुनाएँ जो सिखाएँ कि दूसरों की आलोचना करने के बजाय आत्मसुधार महत्वपूर्ण है।
वयस्कों के लिए समाधान
यदि कोई व्यक्ति पहले से ही इस मानसिक समस्या से ग्रस्त है, तो निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं:
आत्मविश्लेषण करें: अपनी आलोचनात्मक प्रवृत्ति को पहचानें और धीरे-धीरे इसे कम करने का प्रयास करें।
संतुलित सोच विकसित करें: दूसरों की केवल कमियाँ न देखें, बल्कि उनकी अच्छाइयों पर भी ध्यान दें।
आत्मसुधार पर ध्यान दें: स्वयं को विकसित करने में अधिक समय लगाएँ बजाय इसके कि दूसरों की गलतियों पर ध्यान दें।
मनोचिकित्सक या काउंसलर की सलाह लें: यदि यह समस्या अत्यधिक हो चुकी है, तो विशेषज्ञ की मदद लें।
सच में दोषी लोगों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण
यह भी आवश्यक है कि हम परदोषदृष्टि से बचें, लेकिन साथ ही अति सहिष्णु भी न बनें। यदि कोई सच में अनैतिक या गलत कार्य कर रहा है, तो उसे अनदेखा करना भी उचित नहीं। संतुलन बनाए रखना आवश्यक है:
तथ्यों पर ध्यान दें: किसी व्यक्ति को दोषी मानने से पहले उसके कार्यों की वास्तविकता को जाँचें।
न्यायसंगत प्रतिक्रिया दें: यदि कोई गलत कर रहा है, तो उसे सुधारने का प्रयास करें, न कि केवल आलोचना करें।
व्यक्तिगत आक्रोश से बचें: किसी व्यक्ति की बुराई को व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित होकर न देखें, बल्कि निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाएँ।
और अंत में….
परदोषदृष्टि केवल एक मानसिक प्रवृत्ति नहीं, बल्कि एक गहरी समस्या है, जो व्यक्ति, परिवार और समाज को प्रभावित कर सकती है। यदि हम इसे समय रहते पहचानकर सुधारने का प्रयास करें, तो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी, बल्कि समाज में भी सकारात्मकता का संचार होगा। आध्यात्मिकता, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है और एक संतुलित, सकारात्मक जीवन जिया जा सकता है। साथ ही, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संतुलन बनाए रखते हुए सचमुच के दोषियों के प्रति सहिष्णुता की अति न करें और उचित न्याय दृष्टिकोण अपनाएँ। अंततः तात्पर्य यही है कि स्वस्थ मन ही स्वस्थ व्यक्तित्व का घटक होगा तथा स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकेगा।